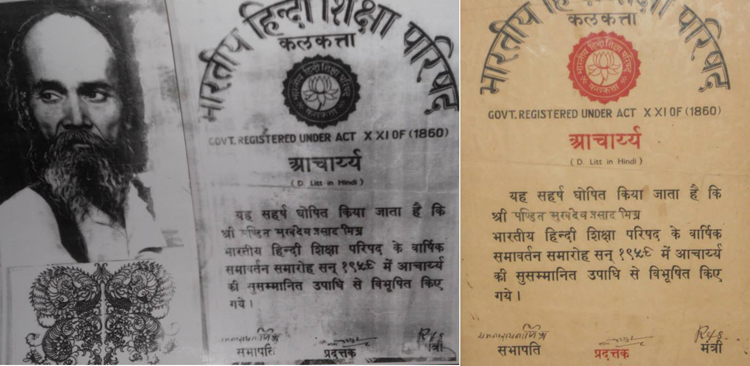बीते दिनों विजया मेहता का नाटक ‘हमीदाबाई की कोठी’ देख रही थी, उसमें हमीदाबाई का एक संवाद है, “आवाज़ अल्लाह देता है, हर एक की आवाज़ अलग होती है। जब तक अल्लाह मियाँ की मर्जी होगी, ये जान रहेगी, आवाज़ रहेगी। अल्लाह मियाँ की इस देन, इस आवाज़ का रिकॉर्ड निकालना अल्लाह मियाँ से बेईमानी है। जब आवाज़ नहीं रहेगी… आवाज़ की याद रहेगी।”
रसूख़ वाली गायिका के यह विचार हो सकते हैं, लेकिन तब यह भी कौंधा कि शायद इस तरह के विचार उस ज़माने के आला दर्जे के कई अन्य गायकों-वादकों, नर्तकों के भी रहे होंगे। तभी तो हमें पुरानी चीज़ें कई बार कहीं नहीं मिलतीं और हम उन लोगों की कला की याद को किस्सों-कहानियों में ही सुना करते हैं। ऐसे ही एक महान् तबला वादक होकर गए हैं जहाँगीर खाँ साहब। उनका जन्म भले ही वर्ष 1869 में हुआ हो लेकिन उनकी मृत्यु 11 मई 1976 में हुई और तब तक कई रिकॉर्ड कंपनियाँ अपने कदम जमा चुकी थीं… बावजूद उनका बजाया सुनने के लिए उनके पहले पंक्ति के शार्गिदों को ही खोजना पड़ता है और उनमें से भी कई अब या तो नहीं रहे या उम्र के उस पड़ाव पर पहुँच गए हैं जहाँ यदि उनकी बातों को न सहेजा गया तो यह हमारा ही नुकसान होगा। जहाँगीर खाँ साहब के वादन की एक रिकॉर्डिंग प्रसार भारती के दिल्ली आकाशवाणी केंद्र में सहेजी हुई है लेकिन बस उतना ही!
पिता जनाब अहमद खाँ साहब से तबले की विरासत को पाकर गुणग्राही जहाँगीर खाँ साहब ने पटना के मुबारक अली खाँ, बरेली के छन्नू खाँ, दिल्ली के फिरोजशाह और लखनऊ के खलीफा आबिद हुसैन खाँ साहब से तबले की घरानेदार शैलियों की विशेषताओं को सीखा, आत्मसात् किया। संगीत सम्राट उस्ताद रज्जब अली खाँ साहब के साथ उन्होंने वर्षों संगत की।
इंदौर के महाराजा तुकोजीराव होलकर ने वर्ष 1911 के आस-पास आपको अपने दरबार के अन्य प्रतिष्ठित कलाकारों के साथ नियुक्त किया। इस बारे में उनके शिष्यों में अग्रणी पंडित दिनकर मुजूमदार बताते हैं- “होलकर स्टेट में तब महीने भर सांगितिक आयोजन होते थे, जिसमें वे आए थे और फिर यहीं (इंदौर) के होकर रह गए। बनारस के पास के एक गाँव के मूल निवासी जहाँगीर साहब की उसी गाँव में पहले ही शादी हो गई थी। उनके दो बेटे भी थे, लेकिन इंदौर आने के बाद उन्होंने फिर कभी उधर का रूख नहीं किया। स्टेट की दरबारी गायिका के साथ उन्होंने संगत की और फिर उसे ही अपनी जीवन संगिनी बना लिया। उनसे कोई संतान न हुई। दरबारी गायिका की मृत्यु के बाद भी वे दरबार में संगत करते थे, बाद में उन्हें दरबार से पेंशन मिलती थी। संगतकार का जीवन बिना किसी के साथ के अधूरा हो गया था…उन्होंने फिर एक निकाह किया जिससे बेटा मुमताज़ हुआ। वह न्यायालय में नौकरी करता था लेकिन अब उसकी भी मृत्यु हो गई है। वैसे भी मुमताज़ ने ज़्यादा नहीं सीखा था, उसे किसी ने कह दिया था कि तबला सीखा तो कोठे पर बजाना होगा तो उसने तबला बजाना छोड़ दिया था।”

ऐसे में खाँ साहब की तबले की विरासत सही मायनों में उनके शिष्यों ने ही संभाली। जहाँगीर खाँ साहब शिक्षा देने में बहुत उदार थे। उनके प्रमुख शिष्यों में नारायण राव इंदूरकर, महादेव राव इंदूरकर, गजानन ताड़े, शरद एवं माधव खरगोणकर, रवि दाते, दिनकर मुजूमदार एवं दीपक गरुड़ हैं। मुजूमदार साहब पर तो खाँ साहब का इतना स्नेह था कि वे मुजूमदार साहब के रेशम वाली गली के घर पर लगभग रोज़ शाम चार-पाँच बजे आते थे, और आवाज़ लगाते “अरे भैया! मोजमदार”, फिर उन्हें ‘बाबा’ कहकर लाड़ से सिखाते और बैठक चल पड़ती। गुरु से सीखने का सबब मुजूमदार साहब के घर में इस तरह की रवायत बन गई कि यह कहने में ज़रा भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बिल्कुल कल-परसों तक भी उनके घर में नियम से दोपहर साढ़े तीन बजे चाय का पानी चढ़ जाता था और चार बजे से रियाज़ शुरू! इस बात पर 90 वर्ष के होने जा रहे मुजूमदार साहब ज़ोर से ठहाका लगाते हुए कहते हैं “सब उस्ताद जी का दिया है। अपनत्व इतना था कि एक बार हमेशा ही रहने के लिए आ गए थे। तब उस्ताद जी को समझाया, उन्होंने खाना खाया… तब तक बेटा मुमताज भी उन्हें लिवाने आ गया और फिर उस्ताद साहब अपने घर लौटे। वे केवल मुझे ही नहीं सीखाते थे, अन्य जो भी गुरु बंधु आते थे, वे उन्हें भी साथ में तालीम देते।”

गुरु बंधू अनिल ओकदे (77 वर्ष) कहते हैं कि हम जब चाहें मुजूमदार साहब के घर पहुँच जाते थे और आवाज़ देते “दीनू भैया, नीचे आ जाओ… तबला सीखना है आपसे। दीनू भैया भी बड़े बंधू की तरह ही सब सीखाते। गुरु के सामने किस तरह से बैठना, गुरु के आने पर उठकर खड़े होना, गुरु का कहा सुनना और बीच में कुछ नहीं बोलना… और ज़्यादा तो कदापि नहीं बोलना। कितने ही मूलमंत्र दीनू भैया ने ही हमें दिए।”
अपनी तालिम के बारे में अनिल जी बताते हैं “पुणे के रवि दाते जी का वादन रावजी भवन इंदौर में हुआ था। उसे सुनने के बाद लगा कि मुझे भी उस्ताद जी से गंडा बँधवा लेना चाहिए। रेशम वाली गली में मेरा भी घर था और मुझसे अगली गली में दीनू भैया रहते थे। मुझे पता चला कि उस्ताद जी उनके यहाँ रोजाना आते हैं तो मैं भी चला आया… मन में एक ही लौ थी कि गंडा बँधवाना है। यह बात वर्ष 1961 की है। मैं नौकरी करता था और घर में कोई सांगितिक विरासत भी नहीं थी लेकिन जाने क्या हुआ कि लगा कि मुझे सीखना ही है। उस्ताद जी ने भी मेरे भीतर की आग को भाँप लिया होगा और उन्होंने हामी भर दी। उस्ताद साहब ने खुद मेरे साथ चलकर तबले की जोड़ खरीदवाई थी।”
दरअसल हमें दीनू भैया को कभी भी गुहार लगाकर कुछ सीखाने की माँग करने की जो आदत लगी थी वह भी उस्ताद साहब की ही देन है। वे बड़ी उदारता से सीखाते थे। कभी-कभी सुबह दस-साड़े दस बजे आ जाते, मुझे दफ्तर जाना होता था लेकिन वे कहते- बाबा बजा लो कुछ। वे सारे शिष्यों को प्यार से बाबा ही कहते थे। वे कहते, बाबा सीख लो कोई नहीं बताएगा.. दीनू भैया ने भी बहुत साथ दिया। दीनू भैया के रेशम वाली गली के घर में उस्ताद साहब ने तबले के बोल किस तरह से निकलना चाहिए, किस ढब से बजाना चाहिए जैसी कई बातें सिखाई। उन्हें लगता था कि मेरा हाथ अच्छा है और गंभीरता से मैं सीखना चाहता हूँ तो उन्होंने तालीम देना शुरू किया। पूरब अंदाज में उनसे सीख रहा था। लटके-झटके से वे कोसों दूर थे, कंधे उचकाकर बजाना उन्हें बिल्कुल पसंद न था। यदि इस बीच कोई आ जाता तो वे यदि कुछ घरानेदार सीखा रहे होते तो तुरंत बंद करने के लिए कह देते थे कि कहीं कोई घरानेदार चीज़ न उठा ले। वे पढंत करवाते, वज़न समझाते, बोल अपने सामने बैठ लिखवाते। हाथ रखने का तरीका सीखाते। दीनू भैया तो ग्वालियर में सामता प्रसाद जी तक के सामने तबला बजा चुके थे, मैं पूरी तरह नया था.. लेकिन अगले 12 साल उनसे सीखता रहा। उसके आगे के भी साल जब तक वे जीवित थे मैं नियमित उनके मोती तबेला के घर पर जाया करता था…और अब उनकी बातें याद आती हैं जिसे उनके बाद वास्तव में किसी और ने कभी नहीं बताया…